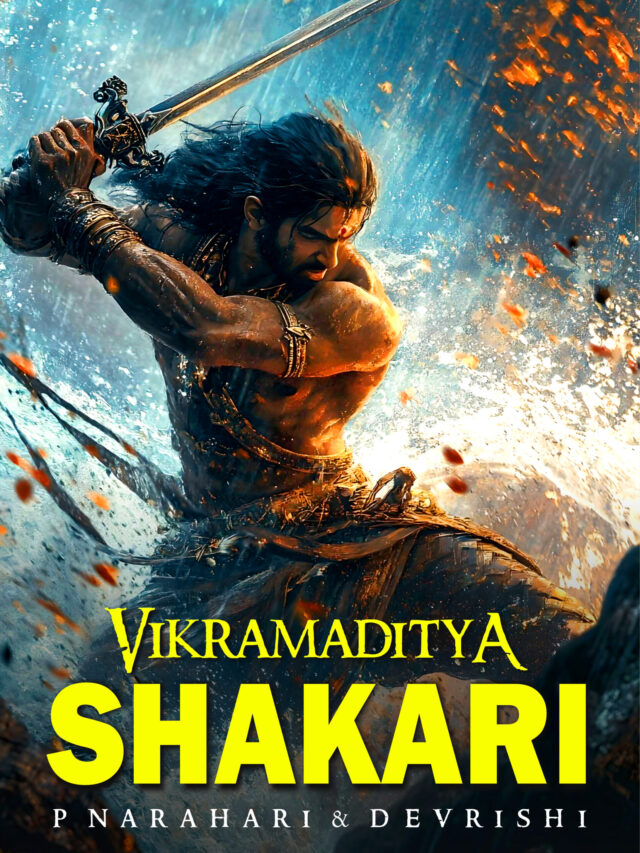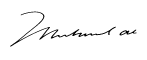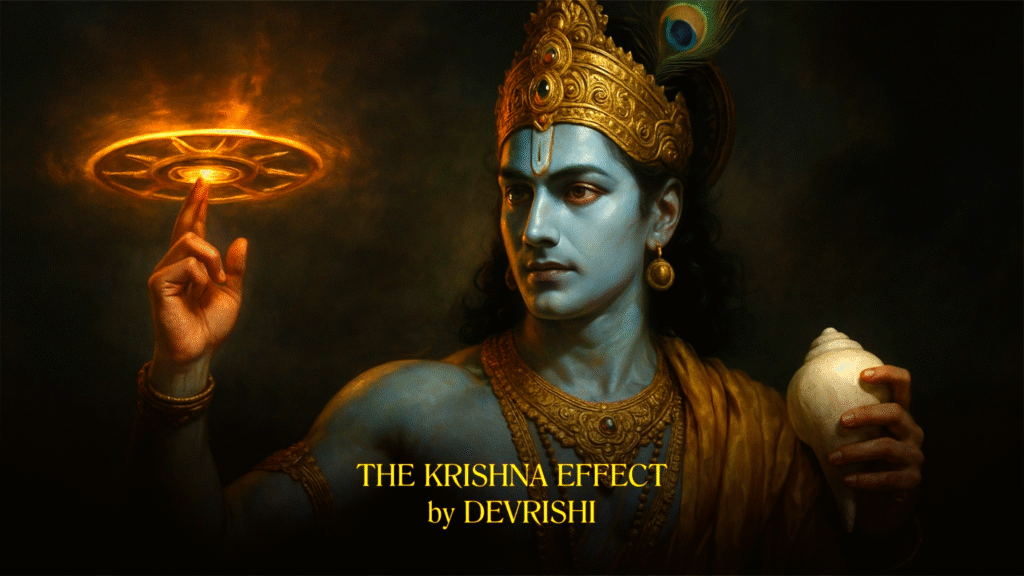हर कार्तिक अमावस्या को पूरे भारत में मनाया जाने वाला यह दीपों का पर्व, लोकप्रिय पौराणिक कथाओं से कहीं अधिक जटिल और आकर्षक इतिहास रखता है। पुरातात्विक साक्ष्य, पाठ विश्लेषण और विद्वतापूर्ण शोध से 2,000 वर्षों के विकासक्रम का पता चलता है जो सरल आख्यानों को चुनौती देता है—जिसमें मूल रामायण में ही दीवाली के उल्लेख की चौंकाने वाली अनुपस्थिति भी शामिल है।
दीवाली लाखों दीयों से भारत के हर कोने को आलोकित करती है, लेकिन इस प्रिय पर्व की उत्पत्ति विद्वानों की बहस और ऐतिहासिक परतों में छिपी रहती है। जबकि अधिकांश भारतीय दीवाली को भगवान राम की अयोध्या वापसी से जोड़ते हैं, शैक्षणिक अनुसंधान एक आश्चर्यजनक तथ्य उजागर करता है: वाल्मीकि रामायण में दीवाली का कोई उल्लेख ही नहीं है। इसके अलावा, महाकाव्य के अनुसार, राम चैत्र मास (मार्च-अप्रैल) में अयोध्या लौटे थे, न कि कार्तिक (अक्टूबर-नवंबर) में जब दीवाली मनाई जाती है—यह छह महीने की विसंगति दशकों से विद्वानों को हैरान करती रही है। यह कालक्रम संबंधी रहस्य भारत के सबसे बड़े त्योहार की समृद्ध बुनावट में एक धागा मात्र है, जिसकी असली उत्पत्ति फसल परंपराओं, देवी पूजा, क्षेत्रीय विविधताओं और दो सहस्राब्दियों में फैली क्रमिक पौराणिक परतों के जटिल अंतर्संबंध में निहित है।
प्राचीन जड़ें धार्मिक आख्यानों से पहले की हैं
दीवाली जैसे पर्व का सबसे पहला प्रलेखित संदर्भ वात्स्यायन के कामसूत्र (तीसरी शताब्दी ईस्वी, लगभग 50-400 ईस्वी) में मिलता है, जहाँ इसे “यक्षरात्रि” कहा गया है—यक्षों की रात, जो धन के देवता कुबेर के अधीन प्रकृति आत्माएं हैं। यह प्राचीन ग्रंथ पंक्तियों में दीप प्रज्वलित करने, अलाव और जुए का वर्णन करता है—मूल तत्व जो आधुनिक दीवाली समारोहों में आज भी बने हुए हैं। 12वीं शताब्दी के जैन विद्वान हेमचंद्र ने बाद में अपने कोश देसी-नाम-माला में यक्षरात्रि को स्पष्ट रूप से दीवाली के साथ समतुल्य बताया, जिससे भाषाई निरंतरता स्थापित हुई।
यह संदर्भ राम के साथ जुड़ाव से कई शताब्दियों पहले का है, जो पी.के. गोडे की 1945 की अभूतपूर्व थियरी का समर्थन करता है कि दीवाली की उत्पत्ति उत्तर भारत में एक कृषि फसल त्योहार के रूप में हुई थी। गोडे, जिनका अध्ययन “हिंदू त्योहारों के इतिहास का अध्ययन” भंडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान के इतिहास में प्रकाशित सबसे व्यापक शैक्षणिक विश्लेषण बना हुआ है, ने 50 ईस्वी से 1945 तक त्योहार के विकास को प्रलेखित किया। उनकी क्रांतिकारी कालानुक्रमिक पद्धति ने खुलासा किया कि दीवाली समारोह धान-फसल की कटाई के अंत और सर्दियों की शुरुआत के साथ मेल खाते थे—महत्वपूर्ण कृषि संक्रमणों को चिह्नित करते हुए जो समुदाय के अस्तित्व को निर्धारित करते थे।
स्वदेशी समुदायों से प्राप्त साक्ष्य इस कृषि मूल का समर्थन करते हैं। बस्तर आदिवासी समुदाय धान की कटाई के बाद डेढ़ महीने तक “दियारी तिहार” मनाता है, जबकि मध्य प्रदेश के दही क्षेत्र की जनजातियाँ दो महीने तक दीवाली मनाती हैं, जिसका समय चंद्र गणनाओं के बजाय फसल पूर्णता से निर्धारित होता है। ये समुदाय पशुधन पूजा और कृषि समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो विद्वानों का मानना है कि त्योहार का सबसे आदिम रूप हो सकता है।
कश्मीर के नीलमत पुराण (छठी-सातवीं शताब्दी ईस्वी) में दीवाली का देवी लक्ष्मी के साथ पहला स्पष्ट पाठ्य संबंध मिलता है, जो त्योहार को “सुखसुप्तिका-दीपमाला” (सुख से सोने के लिए दीपों की पंक्तियाँ) के रूप में वर्णित करता है और कार्तिक के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर लक्ष्मी पूजा निर्धारित करता है। सातवीं-दसवीं शताब्दियों तक, स्कंद और पद्म पुराण जैसे प्रमुख पुराणों ने विस्तृत अनुष्ठानों को संहिताबद्ध कर दिया था, जिससे आज परिचित पाँच दिवसीय त्योहार संरचना ठोस हो गई।
पुरातात्विक शिलालेख 10वीं शताब्दी तक व्यापक उत्सव की पुष्टि करते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य के ताम्रपत्र (939-967 ईस्वी) में “दीपोत्सव” का उल्लेख है, जबकि धारवाड़ के 1119 ईस्वी के कन्नड़ शिलालेख में स्पष्ट रूप से “दीपावली” को “पवित्र अवसर” बताया गया है। शायद सबसे मार्मिक 13वीं शताब्दी का श्रीरंगम, तमिलनाडु के रंगनाथ मंदिर का शिलालेख है, जो दीवाली को “प्रकाश का शुभ त्योहार जो सबसे गहन अंधकार को दूर करता है, जिसे पूर्व दिनों में राजा इल, कार्तवीर्य और सगर ने मनाया था” के रूप में वर्णित करता है। ये पाषाण अभिलेख प्रदर्शित करते हैं कि मध्ययुगीन काल तक, दीवाली राजकीय संरक्षण के साथ एक अखिल भारतीय उत्सव बन चुकी थी।
रामायण विरोधाभास: छह महीने का अंतराल
यहाँ दीवाली की सबसे दिलचस्प विद्वतापूर्ण पहेली है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड (श्लोक 6.124-126) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राम चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 5वीं या 6वीं तिथि को, पुष्य नक्षत्र में अयोध्या लौटे थे—जो मार्च-अप्रैल के अनुरूप है, न कि अक्टूबर-नवंबर का। पाठ में वर्णन है कि राम रावण को मारने के लगभग पाँच से दस दिन बाद ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे, पुष्पक विमान से तीव्र गति से यात्रा करते हुए।
अधिक महत्वपूर्ण रूप से, रामायण में दीप प्रज्वलित करने, दीयों से जश्न मनाने, या राम के स्वागत के दौरान किसी दीपावली पालन का कोई संदर्भ नहीं है। सहपीडिया और द वायर के 2025 के विश्लेषण के अनुसार, “रामायण या यहाँ तक कि तुलसीदास की रामचरितमानस में भी दीवाली या दीपावली का कोई संदर्भ नहीं है।” युद्ध कांड में संरक्षित भरत के राम स्वागत निर्देशों में सुगंधित मालाओं और संगीत वाद्ययंत्रों के साथ देवताओं की पूजा का उल्लेख है, सैनिकों और नागरिकों के राम के चेहरे को “चंद्रमा की तरह” देखने के लिए जाने का—लेकिन मिट्टी के दीपों की पंक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है जो दीवाली को परिभाषित करती हैं।
रॉबर्ट पी. गोल्डमैन जैसे पाठ्य विद्वान, जिन्होंने 2016 में पूर्ण हुए वाल्मीकि रामायण के आलोचनात्मक संस्करण अनुवाद का नेतृत्व किया, सबसे प्राचीन और विश्वसनीय पांडुलिपियों में इस अनुपस्थिति की पुष्टि करते हैं। कालक्रम संबंधी असंभवता ने मध्यकालीन विद्वानों को भी परेशान किया—यदि रावण को आश्विन मास में मारा गया था (जैसा कि विजयादशमी पर मनाया जाता है), और राम तुरंत बाद लौट आए, तो उत्सव कार्तिक अमावस्या, 20 दिन बाद, कैसे स्थानांतरित हो गया?
विद्वानों का सर्वसम्मत मत, जिसे गोडे ने सबसे बलपूर्वक व्यक्त किया और समकालीन शोधकर्ताओं ने समर्थन दिया, यह है कि राम-दीवाली संबंध एक पूर्व-विद्यमान मौसमी त्योहार पर मध्यकालीन पौराणिक परत का प्रतिनिधित्व करता है। यह संबंध रामायण की रचना (5वीं-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी) और दीवाली की शरद ऋतु प्रकाश त्योहार के रूप में स्थापना, दोनों के शताब्दियों बाद बनाया गया प्रतीत होता है। उत्तर भारत ने, अयोध्या के साथ अपनी क्षेत्रीय पहचान और भक्ति आंदोलन के राम पूजा के लोकप्रियकरण के साथ, धीरे-धीरे इस आख्यान को अपनाया, ऐतिहासिक सटीकता पर प्रतीकात्मक अर्थ को प्राथमिकता देते हुए।
विद्वान नताशा मिकल्स एक सम्मोहक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती हैं: “दीवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी व्याख्याओं की बहुलता का एक संभावित उत्तर हो सकता है: कि उत्पत्ति का आख्यान अनुष्ठानों के बाद का विचार है।” अनुष्ठान प्रथाएं—फसल के समय दीप प्रज्वलित करना, धन देवताओं की पूजा करना, जुआ खेलना, भोज करना—पहले अस्तित्व में थीं। समुदायों ने बाद में मौजूदा रीति-रिवाजों की व्याख्या और समृद्धि के लिए सार्थक पौराणिक कथाएँ जोड़ीं।
बंगाल की उग्र देवी: जब काली लक्ष्मी को ग्रहण करती हैं
जबकि भारत का अधिकांश हिस्सा दीवाली की रात सौम्य लक्ष्मी की पूजा करता है, बंगाल भयावह फिर भी प्रिय काली की आराधना करता है—एक विचलन जो गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक भेदों को प्रकट करता है। यह क्षेत्रीय भिन्नता आश्चर्यजनक रूप से हालिया है, जो मुख्य रूप से 18वीं-20वीं शताब्दियों के दौरान उभरी है न कि एक प्राचीन विभाजन का प्रतिनिधित्व करती है।
इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे नदिया के राजा कृष्णचंद्र (1710-1783), जिन्होंने काली पूजा को श्मशान भूमि में किए जाने वाले गुप्त तांत्रिक अभ्यासों से दीवाली की रात के भव्य सार्वजनिक समारोहों में परिवर्तित कर दिया। कृष्णचंद्र से पहले, काली पूजा गूढ़ थी, मुख्य रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती थी। राजा, जिन्हें इतिहासकार अतुल चंद्र रॉय ने “बंगाल के हिंदू समाज में उस काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति” बताया है, ने विस्तृत अनुष्ठान स्थापित किए जो गृहस्थ कर सकते थे, मंदिर संरक्षण और अनुष्ठान संहिताकरण के माध्यम से संस्थागत समर्थन बनाते हुए।
कोलंबिया विश्वविद्यालय की बंगाली देवी पूजा पर अग्रणी विद्वान राहेल फेल मैकडर्मॉट नोट करती हैं कि “पाठ्य साक्ष्य सुझाव देते हैं कि बंगाली हिंदू औपनिवेशिक युग से पहले लक्ष्मी की पूजा करते थे, और काली पूजा एक अधिक हालिया घटना है।” काली पूजा का पहला अनुष्ठान ग्रंथ, काशीनाथ का श्यामासपर्याविधि, केवल 1777 में प्रकट हुआ। सार्वजनिक (समुदाय) काली पूजा परंपरा 1920 के दशक के मध्य के बाद ही व्यापक बनी, जिससे यह बड़े पैमाने पर 20वीं शताब्दी की घटना बन गई।
धार्मिक भेद गहरा है। लक्ष्मी, वैष्णव ढांचे में, सौम्य समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं—भौतिक प्रचुरता जो धार्मिक जीवन का समर्थन करती है। वे दिव्य स्त्री शक्ति के संरक्षण पहलू को मूर्त रूप देती हैं, जो कृषि बहुतायत, घरेलू सुख और स्थिर धन संचय से जुड़ी हैं। दीवाली पर उनकी पूजा शुभता और नई शुरुआत पर बल देने वाली मुख्यधारा की ब्राह्मणिक परंपराओं को दर्शाती है।
काली, बंगाल की प्रमुख शाक्त परंपरा में, कुछ कहीं अधिक कट्टरपंथी का प्रतिनिधित्व करती हैं। खोपड़ियों की माला, बाहर निकली रक्त-सनी जीभ, और शिव के लेटे शरीर पर खड़ी अपनी काली आकृति के साथ, वे कच्ची परिवर्तनकारी शक्ति को मूर्त रूप देती हैं जो मुक्त करने के लिए नष्ट करती हैं। कालीकुल तंत्र दर्शन में, काली परम वास्तविकता हैं—स्वयं समय (काल), पारंपरिक नैतिकता से परे शून्य, उग्र माँ जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अहंकार और अज्ञान को नष्ट करती हैं। अमावस्या, सबसे अंधेरी रात को, आधी रात में उनकी पूजा, श्मशान वास्तविकता में मृत्यु, भय और भ्रम के विघटन का सामना करने का प्रतीक है।
यह विचलन कई कारकों से आकार ली गई बंगाल के अनोखे आध्यात्मिक परिदृश्य को दर्शाता है: पाल वंश (8वीं-12वीं शताब्दी) द्वारा बंगाल को प्रमुख शक्ति पूजा केंद्र के रूप में स्थापना; आर्य प्रभाव से पहले की मजबूत स्वदेशी देवी परंपराएँ; मुगल युग के संरक्षण नेटवर्क जो धनी जमींदारों को विशिष्ट त्योहारों को प्रायोजित करने में सक्षम बनाते हैं; बंगाल पुनर्जागरण का काली को शक्ति और उपनिवेश-विरोधी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उन्नयन; और रामप्रसाद सेन (1718-1775) जैसे भक्ति कवि जिन्होंने भयावह देवी को “मा”—कोमल माँ—में बदल दिया, सुलभ श्यामा संगीत कविता के माध्यम से।
महत्वपूर्ण रूप से, दोनों देवियाँ समृद्धि और शक्ति से संबंधित हैं, लेकिन अलग तरीके से: लक्ष्मी धर्मपरायण जीवन को सक्षम करने वाली भौतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं; काली भौतिक बंधन से परे आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करती हैं। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में, यह संश्लेषण स्पष्ट हो जाता है—काली को दीवाली के दिन लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, जो इन्हें एक ही दिव्य स्त्री शक्ति के पूरक पहलुओं के रूप में प्रकट करता है।
विद्वानों के दृष्टिकोण: अनेक सत्य, एक त्योहार
इतिहासकारों, मानवविज्ञानियों और धार्मिक अध्ययन विद्वानों द्वारा दशकों के शोध से संश्लेषित समकालीन शैक्षणिक समझ, एकल “सच्ची” दीवाली उत्पत्ति की खोज को अस्वीकार करती है। इसके बजाय, विद्वान त्योहार को एक पैलिम्पसेस्ट के रूप में पहचानते हैं—एक पांडुलिपि जहाँ अर्थ की क्रमिक परतें पहले के ग्रंथों पर अंकित की गई हैं, प्रत्येक समृद्धि जोड़ती है बिना पूरी तरह से पहले की चीज़ों को छिपाए।
डेविड किंसली, जिनका हिंदू देवियों पर काम आधारभूत बना हुआ है, वे धार्मिक दिखने वाले अनुष्ठानों में भी कृषि प्रतीकात्मकता पर जोर देते हैं—गोवर्धन पूजा में उपयोग किया जाने वाला गोबर उर्वरता और फसल चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है, न कि केवल भक्ति भावना। उत्तरी टेक्सास विश्वविद्यालय के पंकज जैन देखते हैं कि यह “असंभव है कि कौन पहले आया, या कितने समय पहले दीवाली शुरू हुई,” यह नोट करते हुए कि सभी कहानियाँ 2,500+ वर्षों में संचित “बुराई पर अच्छाई की जीत” विषय को साझा करती हैं।
जैन दावा दीवाली के सबसे पुराने धार्मिक संबंध पर गंभीर विचार के योग्य है। जैन 527 ईसा पूर्व में कार्तिक अमावस्या पर महावीर के मोक्ष प्राप्ति का जश्न मनाते हैं—एक सत्यापन योग्य तिथि जो पाठ्य हिंदू संदर्भों से शताब्दियों पहले की है। कल्पसूत्र 18 राजाओं द्वारा दीपावली की “आध्यात्मिक प्रथा” की संस्था का वर्णन करता है उस रात जब महावीर ने मुक्ति प्राप्त की। जैसा कि द वायर के 2025 के विश्लेषण का सुझाव है, “दीवाली तब जैन धर्म के प्रभाव का साक्ष्य हो सकती है।”
हालिया अनुभवजन्य शोध दीवाली के सामाजिक कार्य को मान्य करता है। जर्नल ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में 2020 के एक अध्ययन ने दो भारतीय समुदायों में अनुदैर्ध्य रूप से अनुष्ठान भागीदारी को मापा, यह प्रदर्शित करते हुए कि दीवाली अनुष्ठानों में निवेश किया गया समय सीधे बढ़े हुए सामाजिक बंधन, सकारात्मक प्रभाव और व्यक्तिपरक स्वास्थ्य से संबंधित था। यह वैज्ञानिक पुष्टि जो अभ्यासकर्ताओं ने हमेशा जाना है—कि दीवाली सामुदायिक एकता को मजबूत करती है—त्योहार की धार्मिक सीमाओं और भौगोलिक प्रवासों के पार दृढ़ता की व्याख्या करती है।
विद्वान हार्वे व्हाइटहाउस नोट करते हैं कि “हम जो अनुष्ठान करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, उनका मानव सहयोग के लिए बड़े परिणाम हुए हैं,” समूह सीमाओं और वफादारी के रूपों को आकार देते हुए। दीवाली इसका उदाहरण है: चाहे हिंदू राम की वापसी का जश्न मना रहे हों, जैन महावीर के मोक्ष को स्मरण कर रहे हों, सिख गुरु हरगोबिंद की रिहाई को चिह्नित कर रहे हों, या बंगाली काली की पूजा कर रहे हों, पूरे भारत में समुदाय साझा अनुष्ठान शब्दावली—दीप प्रज्वलित करना, परिवार इकट्ठा करना, मिठाई बाँटना, प्रार्थना अर्पित करना—का अभ्यास करते हैं जो मानवविज्ञानी विक्टर टर्नर द्वारा “कम्युनिटास” कहा जाता है, सामूहिक उत्सव के माध्यम से सामान्य सामाजिक पदानुक्रमों का अस्थायी अतिक्रमण।
पर्यावरणीय आयाम समकालीन छात्रवृत्ति का नवीनतम योगदान प्रस्तुत करता है। वासुधा नारायणन नोट करती हैं कि पटाखे, जो अब कई लोगों के लिए दीवाली के पर्याय हैं, अपेक्षाकृत हालिया जोड़ हैं—मुख्य रूप से पिछली शताब्दी के। जैसे-जैसे वायु प्रदूषण हर दीवाली पर उत्तर भारतीय शहरों में संकट स्तर तक पहुँचता है, विद्वान और कार्यकर्ता विस्फोटक आतिशबाजी पर मिट्टी के दीयों पर त्योहार के मूल जोर को पुनर्प्राप्त करने की वकालत करते हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि ऐतिहासिक शोध वर्तमान विकल्पों को कैसे सूचित कर सकता है।
साक्ष्य क्या प्रकट करते हैं
पुरातात्विक निष्कर्षों, पाठ विश्लेषण और विद्वतापूर्ण व्याख्या का संश्लेषण दीवाली को एक जीवित परंपरा के रूप में प्रकट करता है जिसका अर्थ एकल उत्पत्ति से नहीं बल्कि सभ्यताओं में संचित ज्ञान से प्राप्त होता है। त्योहार की संभावना 2,000 साल पहले कृषि संक्रमणों को चिह्नित करने वाले क्षेत्रीय फसल समारोहों के रूप में शुरू हुई थी। कामसूत्र का तीसरी शताब्दी का यक्षरात्रि संदर्भ इस प्रारंभिक चरण को कैद करता है—प्रकाश का एक मौसमी त्योहार, धन पूजा, और सामुदायिक जुआ जो विशिष्ट पौराणिक कथाओं से मुक्त है।
छठी-दसवीं शताब्दी ईस्वी के बीच, पौराणिक साहित्य ने दीवाली के देवी लक्ष्मी के साथ संबंध को संहिताबद्ध किया और विस्तृत अनुष्ठान संरचनाएं स्थापित कीं। इस अवधि में कृषि त्योहारों ने भक्ति परतें प्राप्त कीं, मौसमी धन्यवाद को आध्यात्मिक अभ्यास के अवसरों में बदलते हुए। मध्यकालीन काल ने मौजूदा त्योहार ढांचे पर क्षेत्रीय पौराणिक कथाओं—उत्तर में राम, दक्षिण में कृष्ण, पश्चिम में बलि—के जोड़ने को देखा। इन आख्यानों ने मौजूदा प्रथाओं के लिए सार्थक स्पष्टीकरण प्रदान किए जबकि स्थानीय सांस्कृतिक पहचानों को दर्शाते हुए।
राम की चैत्र वापसी और कार्तिक दीवाली समारोहों के बीच कालानुक्रमिक बेमेल एक समाधान की आवश्यकता वाली समस्या नहीं बल्कि त्योहारों के विकास का साक्ष्य है। समुदायों ने कार्तिक अमावस्या—सबसे अंधेरी रात, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत का पूर्ण प्रतीक है—को व्यावहारिक (फसल के बाद) और प्रतीकात्मक कारणों से चुना, बाद में महत्व को गहरा करने के लिए उपलब्ध पौराणिक कथाओं को जोड़ा। जैसा कि रॉबर्ट फोर्ड कैंपनी देखते हैं, ये आख्यान “तर्क के सूक्ष्म रूपों” के रूप में कार्य करते हैं, यह दावा करते हुए कि अच्छाई आवश्यक रूप से बुराई पर विजय प्राप्त करती है चाहे कोई भी देवता उस विजय को मूर्त रूप दे।
लक्ष्मी-काली विचलन साझा अनुष्ठान ढांचे के भीतर क्षेत्रीय धार्मिक विविधता के लिए हिंदू धर्म की उल्लेखनीय क्षमता को प्रदर्शित करता है। दोनों पूजा रूप प्रामाणिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं से उभरे: धार्मिक जीवन का समर्थन करने के लिए भौतिक समृद्धि चाहने वाले समुदायों के लिए लक्ष्मी; मृत्यु दर का सामना करके भौतिक बंधन से मुक्ति चाहने वालों के लिए काली। राजा कृष्णचंद्र का 18वीं शताब्दी का काली पूजा का परिवर्तन दिखाता है कि व्यक्तिगत एजेंसी और ऐतिहासिक परिस्थिति धार्मिक विकास को कैसे आकार देती है, न कि केवल प्राचीन अधिकार।
आधुनिक छात्रवृत्ति दीवाली के महत्व को कम करने के बजाय समृद्ध करती है इसकी अनुकूली लचीलापन को प्रकट करके—त्योहार जीवित रहा है और फला-फूला है ठीक इसलिए क्योंकि प्रत्येक पीढ़ी मौजूदा संरचनाओं पर नए अर्थों की परतें चढ़ा सकती थी। डायस्पोरा समुदाय ऑकलैंड, टोरंटो और लंदन में नई दीवाली परंपराएं बनाते हैं। पर्यावरण चेतना टिकाऊ समारोहों में नवाचार को प्रेरित करती है। बहुलवादी समाजों में अंतरधर्म पालन त्योहार के जारी विकास को प्रदर्शित करते हैं।
1945 से गोडे की अंतर्दृष्टि भविष्यसूचक बनी हुई है: “हमारे त्योहारों के कालानुक्रमिक खाते के बिना हम उनके इतिहास को नहीं समझ सकते।” फिर भी इस इतिहास को समझना दीवाली को एकल सत्य में हल नहीं करता बल्कि इसकी शानदार जटिलता के लिए सराहना खोलता है—कृषि ज्ञान, भक्ति कविता, तांत्रिक दर्शन, शाही संरक्षण, व्यापारी परंपराएं, आदिवासी रीति-रिवाज, और विद्वतापूर्ण व्याख्या सभी उस त्योहार में योगदान करते हैं जो हर शरद ऋतु में लाखों मिट्टी के दीपों के साथ भारत को रोशन करता है, प्रत्येक लौ एक अनुस्मारक कि ज्ञान अज्ञान को जीतता है, समुदाय अलगाव पर विजय प्राप्त करता है, और प्रकाश हमेशा, अंततः, अंधकार को दूर करता है।
Also Read | श्री कृष्ण का पथ और प्रभाव: वृन्दावन से द्वारका तक