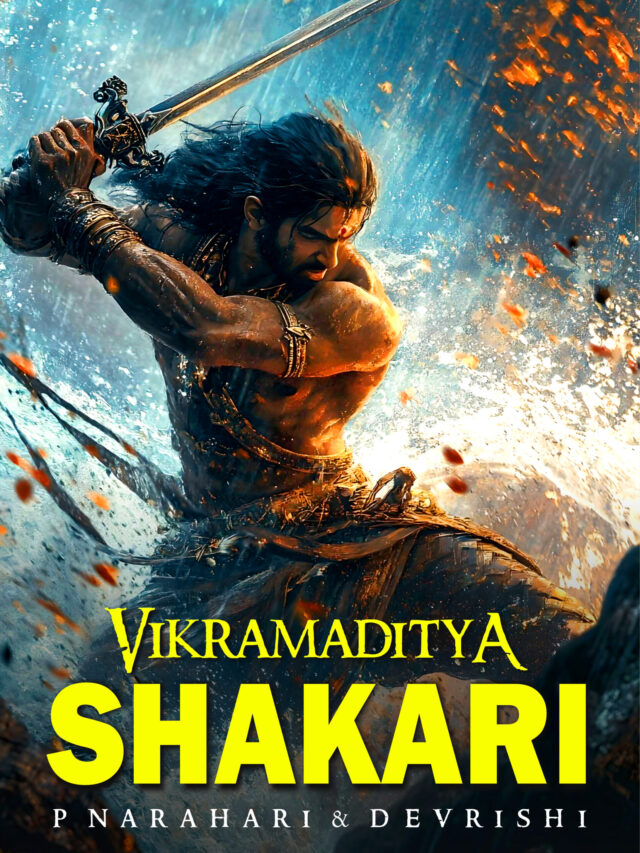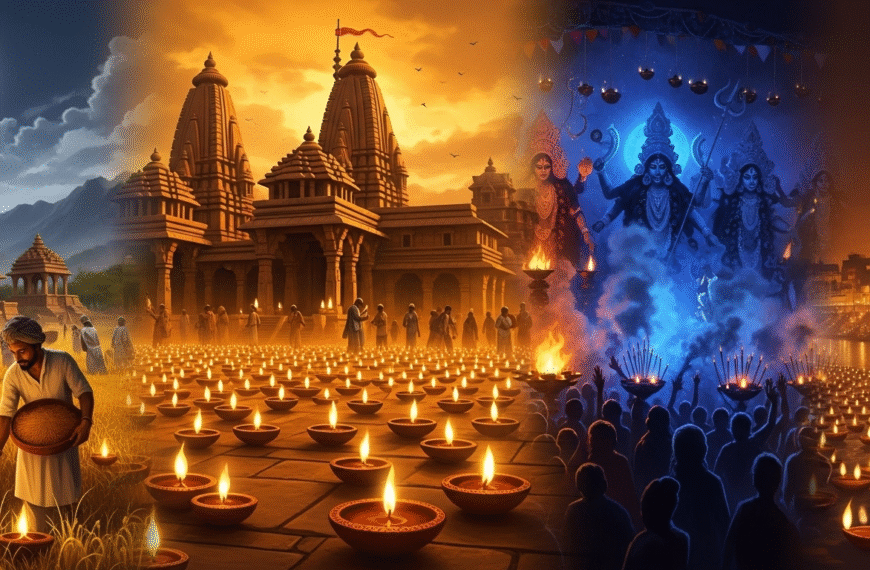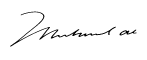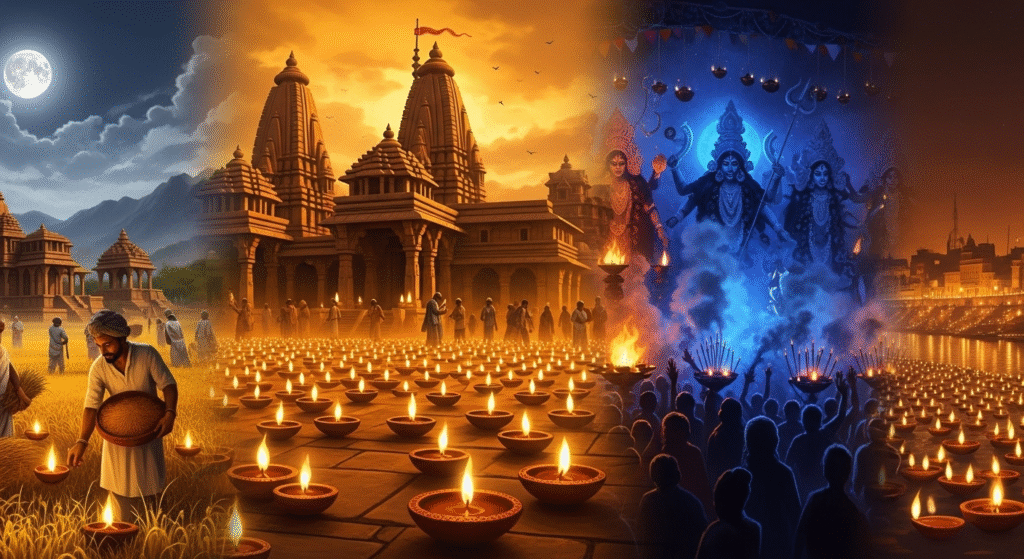इतिहास
नर्मदा भारत की प्राचीन और पूजनीय नदियों में से एक है। इसके उद्गम और महत्व से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएँ मिलती हैं। स्कंदपुराण के रेवा खंड के अनुसार भगवान शिव ने ऋक्ष पर्वत पर तप करते समय अपने पसीने से नर्मदा को उत्पन्न किया, इसलिए इसे शिव की पुत्री भी कहा गया है। एक अन्य कथा में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की दो आँसुओं की बूंदों से दो नदियाँ जन्मी – नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा को प्राचीन ग्रंथों में “रेवा” नाम से भी उल्लेखित किया गया है, जिसका अर्थ इसके चट्टानों पर उछलते प्रवाह (“रेव”) से है। इसे मुक्तिदायिनी देवी के रूप में भी पूजा जाता है, अर्थात “मां नर्मदा” के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। पुराणों में कहा गया है – “गंगा स्नाने, यमुना पाने, नर्मदा दर्शने, ताथा ताप्ति स्मरणे” – यानी गंगा में स्नान और यमुना का जल पीने से जो पुण्य मिलता है, वह नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नर्मदा को हिंदू धर्म में गंगा जैसी ही पवित्र स्थान प्राप्त है। सात प्रमुख पवित्र नदियों (गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, गोदावरी, कावेरी) में नर्मदा को सम्मिलित किया जाता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि नर्मदा ने कभी विवाह नहीं किया और सदैव कुंवारी रही; इसकी पृष्ठभूमि में प्रचलित लोककथा है कि अमरकंटक में उत्पन्न हुए सोनभद्र (सोन नदी) से नर्मदा का विवाह तय था, किंतु सोन के बहक जाने पर नर्मदा क्रोधित होकर पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा की ओर अकेले बह निकली और सदा अविवाहित रहने का प्रण लिया। इसी कथा के कारण नर्मदा को “कुंवारी नदी” के रूप में लोकगीतों में वर्णित किया जाता है।

नर्मदा का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन काल से रहा है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक विभाजक रेखा रही है। प्राचीन औद्योगिक और व्यापारी सभ्यताओं ने इसके किनारे विकसित रूप लिए – जैसे पश्चिम में इसके मुहाने पर स्थित भरूच (प्राचीन भृगुकच्छ) एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जहां से रोमन और ग्रीक लोग भारत से व्यापार करते थे। ईसा की पहली सदी के यूनानी लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इस नदी को “नम्मादियोस” कहा गया है तथा टॉलमी ने “नमदुस” नाम से उल्लेख किया है। मध्यकाल में नर्मदा घाटी में अनेक साम्राज्यों का उदय हुआ। महिष्मती (वर्तमान महेश्वर) का प्राचीन नगर नर्मदा के किनारे स्थित था, जहाँ हैहयवंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन (सहस्रार्जुन) का राज्य था – जिनका वर्णन पुराणों और महाभारत में मिलता है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने महेश्वर को राजधानी बनाकर नर्मदा तट को पुनः गौरवान्वित किया। अंग्रेज़ी काल में भी नर्मदा मध्य भारत की प्रशासनिक सीमा का कार्य करती थी और इसके किनारे कई सैन्य छावनियाँ एवं शहर बसे।
नर्मदा घाटी पुरातात्त्विक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यह भारत में मानव सभ्यता के आदि साक्ष्यों की स्थली है। 1828 में कर्नल विलियम स्लीमैन ने नर्मदा के मध्य प्रवाह क्षेत्र (नरसिंहपुर के पास) में जीवाश्मों की पहली खोज दर्ज की। होशंगाबाद जिले के हथनौरा गांव से मिले एक मानव खोपड़ी के जीवाश्म (जिसे “नर्मदा मानव” कहा जाता है) भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए अब तक के एकमात्र आरंभिक मानव अवशेष हैं, जिससे विश्व मानव-विकास के मानचित्र पर यह क्षेत्र अंकित हुआ। नर्मदा घाटी में पाषाण युगीन उपकरणों से लेकर जीवाश्मों तक, निरंतर उत्खनन होते रहे हैं। देवकछर, बर्मनघाट, मेहदाखेड़ी जैसे स्थलों से हाथी, घड़ियाल, एवं शुतुरमुर्ग के अंडों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययनों में नर्मदा घाटी की सात प्लाइस्टोसीन परतों (पिलिखर, धनी, सुरजकुंड, बनेता, हीरदपुर, बारू और रामनगर फ़ॉर्मेशन) की पहचान की गई है। इन पुरापाषाणीय साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि नर्मदा घाटी मानव पूर्वजों और जीव-जंतुओं के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है। मत्स्य पुराण में नर्मदा के तटों को समस्त तीर्थों के समकक्ष पवित्र बताया गया है और इसके तट को ऋषि-मुनियों की तपोभूमि माना गया। आज भी नर्मदा के तट पर अनेक पुरास्थल, मंदिर एवं प्राचीन अवशेष मिलते हैं जो इसके गौरवशाली अतीत के साक्षी हैं।
भूगोल
नर्मदा मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह मध्यप्रदेश के पूर्वी भाग में विंध्याचल की मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक पठार पर स्थित नर्मदा कुंड नामक जलाशय से उद्गम होती है। अमरकंटक में समुद्र तल से लगभग 1,048 मीटर ऊँचाई पर निकली यह नदी पूर्व से पश्चिम 1,312 किलोमीटर का लंबा मार्ग तय करती है और अन्ततः गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी (अरब सागर) में गिरती है। पूरे प्रवाह के दौरान नर्मदा मध्यप्रदेश में 1,077 किमी, महाराष्ट्र की सीमा पर 74 किमी, तथा गुजरात में लगभग 161 किमी बहती है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बने एक भू-संकुचन (रिफ्ट घाटी) से होकर प्रवाहित होती है। अधिकांश बड़ी भारतीय नदियाँ पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, किंतु नर्मदा पश्चिममुखी है। रिफ्ट घाटी में बहने के कारण नर्मदा अपना विशाल डेल्टा न बनाकर खाड़ी में एस्चुअरी (मुहाना) बनाती है। भूगर्भविदों के अनुसार नर्मदा घाटी बहुत प्राचीन है – यह क्षेत्र लगभग 16 करोड़ वर्ष पूर्व महाद्वीप पैंजिया के विभाजन के समय समुद्री जलमग्न था और बाद में भू-उत्थान से वर्तमान घाटी बनी। इसी कारण इसे विश्व की प्राचीनतम नदियों में से एक माना जाता है।

अपनी लंबी यात्रा में नर्मदा भौगोलिक रूप से विविध प्रदेशों से गुजरती है। अमरकंटक के वनाच्छादित पहाड़ों से निकलकर यह कपिलधारा जलप्रपात के रूप में प्रथम अवतरण करती है। मंडला के पठारी भूभाग से आगे बढ़ते हुए जबलपुर के निकट नर्मदा प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात के रूप में करीब 9 मीटर नीचे गिरती है और वहीं से संगमरमर की चट्टानों की संकरी घाटी बनाती हुई प्रवाहित होती है। भेड़ाघाट (जबलपुर) की इस संगमरमरी घाटी में नदी की चौड़ाई 90 मीटर से सिमटकर मात्र 18 मीटर रह जाती है, जिसे मार्बल रॉक्स के नाम से जाना जाता है। जबलपुर के आगे नर्मदा घाटी फिर चौड़ी होकर नैसर्गिक रूप से तीन बड़े उपघाटियों में विभक्त हो जाती है – पहली घाटी जबलपुर से लेकर होशंगाबाद (नर्मदापुरम) तक, दूसरी वहां से खरगौन ज़िले के महेश्वर क्षेत्र तक और तीसरी आगे गुजरात के भरूच क्षेत्र तक फैलती है। इन घाटियों के बीच-बीच में नदी का पाट कई जगह संकरा होकर पहाड़ियों के बीच से गुजरता है, जिससे अनेक तीव्र मोड़ और छोटे जलप्रपात बनते हैं। मध्य मार्ग में ओंकारेश्वर के पास नर्मदा दक्षिण से आने वाली छोटी कावेरी नदी को अपने में मिलाती है। फिर महेश्वर के पास सहस्रधारा जलप्रपात बनाती हुई यह गुजरात के समतल मैदानों में प्रवेश करती है। गुजरात में भरूच से पूर्व यह फिर चौड़ी होकर विशाल प्रवाह क्षेत्र बनाती है और ज्वारीय प्रभाव वाले मुहाने के रूप में खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा बेसिन (प्रवाह क्षेत्र) लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आवृत करता है, जिसमें विन्ध्य, सतपुड़ा एवं मैकाल पर्वत शृंखला के अनेक उपनद की घाटियाँ शामिल हैं।
नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ दोनो ओर से इसकी जलराशि को समृद्ध करती हैं। पूर्वी मध्यप्रदेश में हिरण, बनजार और शक्कर जैसी नदियाँ उत्तर से इसमें मिलती हैं, तो दक्षिण से तवा सबसे बड़ी उपनदी आकर होशंगाबाद के पास मिलती है। तवा पर बना बड़ा बांध इस जलागम का हिस्सा है (जिसका वर्णन आगे करेंगे)। इसके अलावा दक्षिण से दूधी, शेर, गोई, हथनी इत्यादि नदियाँ एवं उत्तर से बारना, चोरल, ओरसंग आदि नदियाँ नर्मदा में विलय होती हैं। नर्मदा के ऊपरी बेसिन में सुल्तानपुर और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से होकर बहने वाली बंजर और हलोन नदियाँ भी इसकी सहायक हैं। कुल मिलाकर लगभग 41 सहायक नदियाँ नर्मदा में मिलती हैं।

जलवायु प्रभाव: नर्मदा घाटी का जलागम क्षेत्र मुख्यतः मानसूनी जल-प्राप्ति पर निर्भर है। वार्षिक वर्षा का 90% भाग जून-सितंबर के दक्षिण-पश्चिम मानसून महीनों में होता है। नर्मदा के ऊपरी कैचमेंट (अमरकंटक, मंडला क्षेत्र) में घने जंगल और अधिक वर्षा होती है, जबकि निचले क्षेत्र (गुजरात) में अपेक्षाकृत शुष्क जलवायु है। सम्पूर्ण घाटी में प्रायः शुष्क पतझड़ी जंगल पाए जाते हैं, जिसमें सागौन (टीक) प्रमुख वृक्ष है। नर्मदा घाटी का वन क्षेत्र प्राकृतिक रूप से तीन स्तरों वाली वनस्पति वाला है – ऊपरी छतरी में सागौन, बीच में धवड़ा (अनोगीसस लैटिफोलिया), कर्माड (हार्डविकिया) जैसे वृक्ष तथा नदी तट के पास अर्जुन (टर्मिनलिया अर्जुना) और जामुन जैसे सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। नर्मदा के तटीय जंगल जैवविविधता से परिपूर्ण हैं, जिनमें कान्हा और सतपुड़ा जैसे राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं – यहाँ बाघ, बारहसिंगा, घड़ियाल आदि वन्यजीव निवास करते हैं। नर्मदा का विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र मध्यभारत के पूर्वी जंगलों और पश्चिम भारत के शुष्क प्रदेशों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र बनाता है। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण हाल के दशकों में नर्मदा घाटी के वनों में कमी आई है, जिसका प्रभाव नदी के प्रवाह और तटीय क्षरण पर पड़ा है।
संस्कृति
नर्मदा नदी मध्यभारत की जनजातीय और लोकसंस्कृति में रची-बसी है। इसके उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर संगम तक अनेक लोककथाएँ प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध लोककथा के अनुसार नर्मदा और सोन नदियाँ बचपन में अमरकंटक पर्वत पर साथ पली-बढ़ीं और युवावस्था में दोनों ने विवाह का प्रण किया। मार्ग में सोनभद्र नदी नर्मदा की सखी जुहिला पर मोहित हो गया और नर्मदा को भूल बैठा। इस विश्वासघात से क्रुद्ध होकर नर्मदा ने उसी क्षण अकेले आगे बढ़ने का निश्चय किया और पूर्व की जगह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। नर्मदा ने आजीवन विवाह न करने का संकल्प ले लिया और सन्यासिनी-सी निरंतर बहती गई। कहा जाता है तभी से नर्मदा विपरीत दिशा (पश्चिम) को बहने लगी जबकि अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी (पूर्व) जाती हैं। इस कहानी के कारण नर्मदा को “चिरकुमारी” नदी कहा जाता है और उसके त्याग व पवित्रता की चर्चा लोकगीतों में होती है। नर्मदा को शिव-पुत्री मानते हुए इससे जुड़ी एक कहावत प्रसिद्ध है – “नर्मदा के कंकर, उठे शंकर”, अर्थात नर्मदा के हर कंकर (कंकर अर्थात गोल पत्थर) में शिव बसे हैं। दरअसल नर्मदा के तल में पाए जाने वाले अंडाकार क्वार्ट्ज पत्थरों को “बाणलिंग” कहते हैं, जिन्हें शिवलिंग रूप में भक्तों द्वारा पूजा जाता है। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को “नर्मदा जयंती” पर्व मनाया जाता है, जिस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा में स्नान कर नदी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि माघ शुक्ल सप्तमी (जिसे रथ सप्तमी भी कहते हैं) के दिन नर्मदा का अवतरण हुआ था, अतः इस स्नान पर्व से पापों से मुक्ति मिलती है।

नर्मदा के तटों की संस्कृति में आराधना और आस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक त्योहार एवं मेले इस नदी से जुड़े हैं। कार्तिक पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा पर तटवर्ती शहरों – जैसे जबलपुर, होशंगाबाद, नेमावर आदि – में स्नान एवं दीपदान की परंपरा है। संध्या समय कई स्थानों पर “नर्मदा आरती” का आयोजन होता है, जिसमें हरिद्वार की गंगा आरती की तरह नर्मदा तट पर दीपक जलाकर आराधना की जाती है। जबलपुर के ग्वारीघाट तथा नर्मदापुरम (होशंगाबाद) के सेठानी घाट की नर्मदा आरती प्रसिद्ध हो चुकी है, जहाँ सैकड़ों दीपों की ज्योति और श्रद्धालुओं के स्वर माहौल को भक्तिमय बना देते हैं। नर्मदा के तट पर निवास करने वाले आदिवासी समुदायों (जैसे गोंड, बैगा) की लोककथाओं में नर्मदा को मां का दर्जा प्राप्त है। वे नर्मदा को “नरबदा माई” कहकर संबोधित करते हैं और कई लोकगीतों में इसकी महिमा गाते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में नर्मदा के सम्मान में लोकनृत्य, भजन, तथा नौका उत्सवों का आयोजन भी होता है। कुल मिलाकर नर्मदा नदी ने मध्य भारत की लोक संस्कृति, बोलियों और उत्सवों को एक साझा पर्व में बांधा है।
आध्यात्मिक महत्व
नर्मदा केवल भौगोलिक धरोहर ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक आस्था का भी केंद्र है। इसे प्रयाग, काशी, हरिद्वार जैसी मोक्षदायिनी शक्तियाँ प्राप्त हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि गंगा में स्नान करने से और यमुना का जल पीने से जो पुण्य मिलता है, वह मात्र नर्मदा के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए देश भर के तीर्थयात्री नर्मदा को सम्मानपूर्वक “नर्मदा मैया” कहकर प्रणाम करते हैं। नर्मदा के तट पर पूरे मार्ग में अनेकों तीर्थ स्थल और मंदिर स्थापित हैं, जिनका हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। अमरकंटक में स्वयं नर्मदा उद्गम कुंड एक शक्तिपीठ की तरह पूजा जाता है, जहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु जलार्पण करने आते हैं। ओंकारेश्वर (मध्यप्रदेश) में नर्मदा के मध्य द्वीप पर अवस्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बारह ज्योतिर्लिंगों में एक है, जिसकी परिक्रमा करने दूर-दूर से भक्त आते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है, इसलिए वहाँ के उत्तरवाहिनी घाट को अत्यंत पवित्र माना गया है। महेश्वर में नर्मदा किनारे अहिल्येश्वर मंदिर एवं विशाल घाट हैं, जहाँ सहस्त्रों शिवलिंग प्रतिष्ठापित हैं – यह स्थान अपने प्राचीन देवालयों और साहस्रधारा तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट में नर्मदा की धारा के दोनों ओर 64 योगिनी मंदिरों के अवशेष हैं, जिनका संबंध तांत्रिक उपासना से रहा है। इसके अतिरिक्त चित्रकूट पर्वत पर और बड़वानी (मध्यप्रदेश) के राजघाट तथा गुजरात के शुक्लतीर्थ, अंकलेश्वर आदि स्थानों पर भी नर्मदा तट पर मंदिरों का समूह है।

नर्मदा की परिक्रमा हिंदू धर्म में एक अद्वितीय और परम पुनीत तीर्थ माना जाता है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र नदी है जिसकी समूची परिक्रमा (कुल ~2600 किमी) पैदल चलकर की जाती है। मान्यता है कि नर्मदा की परिक्रमा करना परम फलदायी कर्म है, जो जन्म-मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। परिक्रमा पर जाने वाले श्रद्धालु को “परिकर्मावासी” कहा जाता है। परंपरागत रूप से नर्मदा परिक्रमा यात्रा नर्मदा के दक्षिण तट से आरंभ होकर अरब सागर (खंभात की खाड़ी) के मुहाने तक जाती है, फिर नदी का मुहाना पार करके उत्तरी तट के साथ वापस उसी प्रारंभ बिंदु पर समाप्त होती है। परिक्रमा यात्रा में नदी को कहीं भी पार नहीं करने की प्रतिज्ञा ली जाती है, अर्थात पूरे मार्ग में नदी सदैव दाईं ओर (दक्षिण तट पर चलते हुए) या बाईं ओर (उत्तर तट पर लौटते हुए) ही रहती है। पारंपरिक मान्यता है कि स्कंदपुराण के रेवा खंड में स्वयं नर्मदा परिक्रमा का महात्म्य बताया गया है और इसी से प्रेरित होकर यह प्रचलन शुरू हुआ। नर्मदा परिक्रमा सामान्यतः 3 वर्ष, 3 महीने, 13 दिन में पूर्ण होती है। कई तपस्वी और साधु जीवन में कम से कम एक बार यह कठिन तपस्या करते हैं – वे गुजरात के भरूच (जहाँ नर्मदा सागर में मिलती है) से पैदल यात्रा शुरू कर अमरकंटक (उद्गम) तक जाते हैं और फिर वापसी करते हैं। मार्ग में सैकड़ों तीर्थ और घाट आते हैं जहाँ परिक्रमावासियों के ठहरने व भोजन आदि की नि:शुल्क व्यवस्था स्थानीय लोग करवाते हैं। परिक्रमा का मार्ग कठिन है – घने जंगल, पहाड़, रेगिस्तानी मैदान और नगरों से होकर गुजरता हुआ – इसलिए परिक्रमावासी न्यूनतम सामान के साथ संयमपूर्वक यात्रा करते हैं। परिक्रमा मार्ग पर ओंकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट, अमरकंटक, महाराजपुर, नेमावर, छीपानेर, होशंगाबाद, जबलपुर, मैकलेश्वर, भरूच आदि मुख्य पड़ाव स्थल हैं। इन स्थानों पर श्रद्धालु नर्मदा पूजन, आरती एवं स्थानीय धार्मिक कथाओं का श्रवण करते हैं। आज के दौर में भी हर वर्ष हजारों श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा के लिए निकलते हैं – इसे विश्व के सबसे बड़े शांतिपूर्ण समागमों में से एक कहा जाता है।
सरकारी परियोजनाएं
आज़ादी के बाद भारत सरकार ने नर्मदा नदी की विशाल जलराशि का उपयोग सिंचाई व विद्युत उत्पादन हेतु करने की कई योजनाएँ प्रारंभ कीं। 1940 के दशक में ही नर्मदा पर बाँधों की संभावना पर अध्ययन शुरू हुए थे। 1960 तक मध्यप्रदेश और τότε के बंबई राज्य (गुजरात/महाराष्ट्र) द्वारा नर्मदा पर बड़े बांधों की अलग-अलग योजनाएँ बन चुकी थीं, जिसके चलते अंतर्राज्यीय जल-बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए 1969 में नर्मदा जल विवाद अधिकरण (NWDT) का गठन किया गया, जिसने लगभग 10 वर्ष विचार-विमर्श के बाद 1978 में अपना अंतिम निर्णय दिया। अधिकरण के निर्णय के तहत मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के बीच नर्मदा के जल का बंटवारा और बांधों की ऊँचाई आदि मानकों को स्वीकृति मिली। इसके पश्चात नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन कर चरणबद्ध परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। कुल मिलाकर नर्मदा पर लगभग 30 बड़े बांधों का निर्माण प्रस्तावित/निर्मित हुआ, जिसमें कई बहुउद्देशीय (Multi-purpose) योजनाएँ शामिल हैं।

प्रमुख बांध परियोजनाएँ: सरदार सरोवर बांध (गुजरात) नर्मदा पर बनी सबसे विशाल परियोजना है। यह 163 मीटर ऊँचा कंक्रीट गुरुत्व बांध है, जिसे नर्मदा नदी के अंतिम छोर पर नवागाम के निकट बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाटी विकास परियोजना की प्रमुख कड़ी है – इसके विशाल जलाशय से सिंचाई, पेयजल व विद्युत उत्पादन के लाभ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान को मिलते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े कंक्रीट बांधों में गिना जाता है (निर्माण में प्रयुक्त कंक्रीट की मात्रा की दृष्टि से ग्रांड कूली बांध, USA के बाद दूसरा)। सरदार सरोवर जलाशय की अधिकतम जलधारण क्षमता 0.95 लाख करोड़ लीटर से अधिक है। इंदिरा सागर परियोजना (मध्यप्रदेश) नर्मदा पर बना भारत का सबसे बड़ा जलाशय-वाला बांध है। यह बांध 92 मीटर ऊँचा है और इसमें 12.22 अरब घनमीटर पानी संग्रह की क्षमता है। इंदिरा सागर से 1000 मेगावाट जलविद्युत संयंत्र भी संचालित होता है। मध्यप्रदेश में ही जबलपुर के पास बरगी बांध 1980 के दशक में पूरा हुआ, जिससे नर्मदा में पहली बार बड़ी सिंचाई नहरें निकाली गईं। बरगी जलाशय से जबलपुर तथा आसपास के जिलों में खेती को पानी मिलता है और मछलीपालन को बढ़ावा मिला। इसी तरह ओंकारेश्वर बांध (मध्यप्रदेश) व महेश्वर बांध भी विद्युत उत्पादन हेतु बनाए गए हैं (हालांकि महेश्वर परियोजना विवादों के कारण अपूर्ण है)। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी तवा पर होशंगाबाद जिले में 1974 में तवा बांध बनाकर बड़े भू-भाग में सिंचाई सुविधा पहुंचाई गई। कुल मिलाकर, नर्मदा घाटी की जलविद्युत क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और सूखे क्षेत्रों तक इसके पानी को पहुंचाने के लिए व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। गुजरात में सरदार सरोवर से निकाली गई नर्मदा नहर 532 कि.मी. लंबी है, जो कच्छ और सौराष्ट्र जैसे शुष्क क्षेत्रों तक नर्मदा का पानी ले जाकर साढ़े छह हजार से अधिक गाँवों को सींच रही है। इस नहर की एक शाखा राजस्थान के दक्षिणी ज़िलों तक भी जाती है, जिससे मरुस्थली क्षेत्र को जीवनदायी जल मिला है।
सरदार सरोवर परियोजना अपने आरंभ से ही पर्यावरणीय और सामाजिक असर के कारण चर्चा में रही। ऊँचे बांधों से नर्मदा घाटी के बड़े हिस्से जलमग्न हुए, जिसके चलते हज़ारों लोगों के पुनर्वास की चुनौती उत्पन्न हुई। स्थानीय आदिवासी समुदायों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने बांधों के विरोध में आवाज़ उठाई, जिसमें मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) सबसे प्रमुख रहा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने विस्थापित परिवारों के पुनर्स्थापन, जलाशयों से डूबने वाले जंगलों एवं जीव-जंतुओं की रक्षा, तथा वैकल्पिक छोटे बाँधों की वकालत की। 1980-90 के दशक में यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँचा, जिससे विश्व बैंक ने सरदार सरोवर के लिए दिया जा रहा ऋण तक रोक दिया था। अंततः भारत सरकार को अपने संसाधनों से परियोजना पूरी करनी पड़ी और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से चरणबद्ध निर्माण हुआ। बड़े बांधों के कारण नर्मदा के प्रवाह पर निश्चित नियंत्रण स्थापित हुआ है – बाढ़ की आवृत्ति कम हुई है, वहीं सूखे मौसम में नर्मदा का प्रवाह न्यूनतर हो गया है। बांधों से निकली नहरों ने एक ओर हरित क्रांति को नए क्षेत्रों तक पहुँचाया है, तो दूसरी ओर हजारों हेक्टेयर वनभूमि और ग्राम जलमग्न भी हुए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार सरदार सरोवर एवं अन्य बांधों के जलाशयों से क्षेत्र की जलवायु में आर्द्रता बढ़ी है और भूकंपीय खतरे भी उत्पन्न हुए हैं। फिर भी, नर्मदा पर बनी परियोजनाओं को मध्य भारत की “रेखा” कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोगों को पीने का पानी, बिजली और आजीविका प्रदान की है।
नर्मदा परिक्रमा

नर्मदा परिक्रमा एक ऐसी अनूठी धार्मिक परंपरा है, जिसमें श्रद्धालु संपूर्ण नर्मदा नदी की पदयात्रा कर परिक्रमा पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में यह परिक्रमा अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है और प्राचीन काल से ऋषि-मुनि भी यह प्रयास करते आए हैं। परिक्रमा का विधान है कि यात्री नदी के एक किनारे (दक्षिण तट) के साथ-साथ समुद्र तक जाएँ और फिर दूसरा किनारा (उत्तर तट) पकड़कर आरंभ बिंदु पर लौट आएँ। परिक्रमा किसी भी ओर से शुरू की जा सकती है, पर प्रायः लोग अमरकंटक (उद्गम) या भरूच/रामेश्वर (मुहाना) से आरंभ करते हैं। परिक्रमा करते समय पूरे मार्ग में नदी को नाव से भी पार नहीं किया जाता, अर्थात दक्षिण तट पर जाते समय नदी बाईं ओर रहती है और लौटते समय दाईं ओर। यह यात्रा लगभग 2600 किलोमीटर की मानी जाती है और सामान्यतः इसमें 3 वर्ष, 3 महीने, 13 दिन लगते हैं। परिक्रमार्थी साधु संत हों या गृहस्थ भक्त – सभी कठिन तपस्या की तरह इसे पूर्ण करते हैं। मार्ग की कठिनाइयों – जंगल, पहाड़, नदी-नाले – को सहन करते हुए वे न्यूनतम सुविधाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में आने वाले गाँव-शहरों में स्थानीय लोग इनके ठहरने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था परंपरागत रूप से करते आए हैं। कई जगह तो परिक्रमावासियों के लिए अलग “धर्मशाला” या आश्रम बने हुए हैं। परिक्रमा मार्ग पर ओंकारेश्वर, महेश्वर, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, नेमावर, चांदोड़, गरुडेश्वर, अंकलेश्वर, भरूच आदि प्रमुख पड़ाव स्थल आते हैं। हर पड़ाव पर यह यात्री नर्मदा घाट पर स्नान-पूजन करते हैं और स्थानीय तीर्थों के दर्शन करते हैं। परिक्रमा का धार्मिक नियम है कि यात्रा दक्षिण तट पर आरंभ कर उत्तर तट पर पूरी की जाए, पर कुछ भक्त “अर्ध-परिक्रमा” भी करते हैं (केवल एक ओर जाकर वहीं समाप्त कर लेना)। परिक्रमा का सबसे शुभ मुहूर्त कार्तिक महीने को माना गया है; हालांकि लोग व्यक्तिगत संकल्प लेकर वर्षभर में कभी भी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। गुजरात में अंकलेश्वर के पास 14 किलोमीटर की “पंचकोशी उत्तरवाहिनी परikrमा” प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में आयोजित होती है, जिसमें हज़ारों श्रद्धालु एक माह तक चलने वाले मेले में भाग लेते हैं। कुल मिलाकर, नर्मदा परिक्रमा भक्ति, साहस और सहनशीलता का ऐसा संयोजन है जो भक्तों को आत्मशुद्धि और देवी नर्मदा से आध्यात्मिक जुड़ाव का अद्भुत अनुभव प्रदान करता है।
प्रमुख नर्मदा घाट और स्थल
नर्मदा नदी के किनारे अनगिनत घाट स्थित हैं, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख घाटों का विवरण निम्नवत है:
- अमरकंटक (नर्मदा उद्गम कुंड): अमरकंटक मध्यप्रदेश में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित पवित्र तीर्थस्थल है। यही पर माँ नर्मदा एक छोटे कुंड से प्रकट होती हैं। नर्मदा उद्गम कुंड संगमरमर से निर्मित एक सुंदर चबूतरे से घिरा है, जहाँ नर्मदा मंदिर स्थित है। इस कुंड के जल को अत्यंत पवित्र माना गया है और दूर-दूर से यात्री यहाँ स्नान एवं जलभरन करने आते हैं। कुंड से थोड़ा आगे कपिलधारा जलप्रपात है, जिसका संबंध ऋषि कपिल से जोड़ा जाता है। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर परिसर में वार्षिक नर्मदा जयंती मेला भरता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं।
- ओंकारेश्वर घाट: मध्यप्रदेश के खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी एक बड़े दर्रे से गुजरती है, जहाँ एक ओम (ॐ) आकार का द्वीप बनता है। इसी द्वीप पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है – जो बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकार पर्वत पर बने मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को नदी पार करके जाना होता था, हालाँकि अब पुल बन गए हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा उत्तरवाहिनी (उत्तर की ओर बहने वाली) हो जाती है, इसलिए यहाँ के तट विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। मुख्य घाटों में नागर घाट, अभय घाट, गोमुख घाट आदि हैं जहाँ तीर्थयात्री स्नान करते हैं। हर शाम ओंकारेश्वर घाट पर नर्मदा आरती होती है। ओंकारेश्वर के पास नर्मदा पर एक बांध भी बना है, जिसके कारण एक विशाल जलाशय निर्मित हुआ है और नाव द्वारा परिक्रमा मार्ग सुगम हुआ है।
- महेश्वर घाट: महेश्वर (ज़िला खरगौन, म.प्र.) नर्मदा के उत्तरी तट पर बसा एक ऐतिहासिक नगर है, जिसे प्राचीन काल में माहिष्मती के नाम से जाना जाता था। आज महेश्वर अपने शानदार घाटों, मंदिरों और किले के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा किनारे सहस्रधार घाट पर सहस्त्रों छोटे-बड़े शिवलिंग दर्शनीय हैं। यहीं पर देवी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाए गए अनेक मंदिर हैं। शाम के समय महेश्वर घाट पर बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित कर आरती की जाती है, जिसका प्रतिबिंब नर्मदा के जल में बेहद मनोहर दिखता है। महेश्वर अपने हथकरघा महेश्वरी साड़ियों के लिए भी विख्यात है, जिसका आरम्भ अहिल्याबाई ने घाट पर ही बुनकरों को बसाकर किया था।
- भेड़ाघाट (जबलपुर) के घाट: जबलपुर शहर के निकट भेड़ाघाट क्षेत्र में नर्मदा संगमरमर की पहाड़ियों के बीच बहती है। यहाँ धुआंधार जलप्रपात प्रमुख आकर्षण है, जहाँ पानी की फुहार धुएँ जैसी दिखाई देती है। भेड़ाघाट में नर्मदा के दोनों ओर ऊँची चमकदार श्वेत चट्टानों के कारण इसे “संगमरमर नगरी” कहा जाता है। नौका विहार के दौरान इन चट्टानों पर सूर्य किरणों के बदलते रंग पर्यटकों को मुग्ध करते हैं। भेड़ाघाट के पास नर्मदा तट पर छोटे-छोटे घाट बने हैं जहाँ सैलानी उतरकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। इसी क्षेत्र में चौंसठ योगिनी मंदिर भी हैं, जो एक पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर समूह है।
- होशंगाबाद (नर्मदापुरम) सेठानी घाट: होशंगाबाद शहर नर्मदा के विशाल तट पर बसा है। यहाँ का प्रमुख सेठानी घाट 19वीं शताब्दी में स्थानीय धनाढ्य सेठानी द्वारा बनवाया गया था। यह घाट पक्की सीढ़ियों, छतरियों और मंदिरों से युक्त है। होशंगाबाद के सेठानी घाट पर हर साल मकर संक्रांति एवं कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ा स्नान मेला लगता है। ग्रीष्म काल में शिवरात्रि पर भी श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने आते हैं। सांध्य आरती में इस घाट की शोभा देखते ही बनती है।
- भरूच और अन्य घाट: गुजरात में भरूच नगर के पास नर्मदा का विशाल पाट अंतिम बार शांत प्रवाह में दिखता है। यहाँ नर्मदा तट को “नर्मदा तीर्थ” कहा गया है। भरूच के पास अंकलेश्वर में शुक्लतीर्थ नामक स्थान पर नर्मदा का प्रसिद्ध घाट है, जहाँ हर अमावस्या और पूर्णिमा को श्रद्धालु इकठ्ठा होते हैं। यहीं पास में कवि संत दादू दयाल और कबीर से जुड़े स्थल भी हैं। भरूच से नीचे नदी का जल खारा होने लगता है (समुद्र का प्रभाव) और ज्वारीय लहरें दिखाई देती हैं, इसलिए यहीं पर स्नान की समाप्ति मानी जाती है। इस प्रकार, उद्गम से संगम तक नर्मदा के दर्जनों घाट विभिन्न रूपों में श्रद्धा और संस्कृति के केंद्र बने हुए हैं।
सभ्यता पर प्रभाव

नर्मदा नदी ने आदिकाल से लेकर आज तक मानव सभ्यता के विकास को गहराई से प्रभावित किया है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की “जीवन रेखा” कहा जाता है, क्योंकि करोड़ों लोगों का जीवन एवं जीविका इस पर निर्भर है। प्रागैतिहासिक युग में नर्मदा घाटी मानव आवास के प्रारंभिक केंद्रों में थी – पाषाण युगीन उपकरणों और नरकंकाल के जीवाश्म यहां पाए गए हैं, जिससे संकेत मिलता है कि मानव पूर्वज नर्मदा किनारे बसे थे। उपजाऊ घाटी और जल की उपलब्धता ने कृषि के विकास को संभव बनाया और यहीं आदिम स्तनपायी जीवों का भी विकास हुआ। कालांतर में नर्मदा घाटी विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल बनी। उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच यह सेतु का कार्य करती रही – भौगोलिक विभाजक होने के बावजूद दोनों ओर की भाषाओं, रीति-रिवाजों और वाणिज्य का यहां मिलन हुआ। प्राचीन व्यापार मार्ग नर्मदा के सहारे-सहारे चलते थे, जिसमें उज्जयिनी (उज्जैन) और महिष्मती (महेश्वर) जैसे नगरों से होते हुए पश्चिमी समुद्र तक सामान पहुँचा करते थे। यूनानी एवं रोमन यात्री इसी मार्ग से भारत के भीतरी इलाकों तक व्यापार हेतु गए, जिसका प्रमाण उनके द्वारा नर्मदा का उल्लेख करने से मिलता है।
नर्मदा के तटवर्ती नगर समय के साथ फलते-फूलते रहे। मध्यप्रदेश में जबलपुर, होशंगाबाद (नर्मदापुरम), खरगोन (महेश्वर), खंडवा (ओंकारेश्वर) जैसे शहर नर्मदा के कारण ही बस पाए और पनपे। इन शहरों में सामाजिक जीवन नर्मदा के इर्द-गिर्द केन्द्रित रहा – घाटों पर मेल-मिलाप, धार्मिक अनुष्ठान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सामूहिक एकता को मजबूत करते हैं। गुजरात में राजपीपला, अंकलेश्वर और भरूच जैसे शहर नर्मदा के किनारे पल्लवित हुए। भरूच तो प्राचीन काल से अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह रहा है, जहाँ से मसाले, कपास और हाथीदांत जैसी वस्तुओं का निर्यात होता था। नर्मदा ने कृषि एवं सिंचाई द्वारा भी सभ्यता को समृद्ध किया है – इसके जल से मालवा और निमाड़ के सूखे इलाकों में भी हरियाली आई। आधुनिक काल में नर्मदा परियोजनाओं से लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई है और कई नए शहर/कस्बे (जैसे नर्मदा नगर, सरदारनगर) विकसित हुए हैं। नर्मदा के पानी से औद्योगिक नगरों (जैसे इंदौर, बड़ोदरा) को भी जलापूर्ति होती है।
नर्मदा का सामाजिक जीवन पर गहन प्रभाव देखा जाता है। इसकी घाटी में बसने वाले समुदायों के त्योहार, लोकगीत और आस्था इस नदी से जुड़ी है। स्थानीय कहावत है – “नर्मदा किनारे कोई भूखा नहीं सोता” – क्योंकि नदी सभी को मछली, पानी, और उपजाऊ भूमि देकर पालती है। मछुआरे, नाविक, किसान – सभी के लिए नर्मदा आजीविका का स्रोत है। estimates के अनुसार नर्मदा लगभग 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका देती है। एक ओर इसके किनारे आदिवासी अपने पारंपरिक जीवन जीते हैं, तो दूसरी ओर बड़े शहरों में यही नर्मदा “जल-प्रदायिनी” बनकर नहरों के माध्यम से जीवन देती है। नर्मदा घाटी परियोजना के तहत हुए विस्थापन ने सामाजिक ताना-बाना अवश्य प्रभावित किया, पर पुनर्वास ने अनेक ग्रामीणों को नए स्थानों पर बसने का अवसर भी दिया। संस्कृति के स्तर पर देखें तो नर्मदा ने साहित्य और कला को भी प्रेरणा दी है – कालिदास से लेकर आधुनिक साहित्यकारों तक ने नर्मदा के सौंदर्य पर रचनाएँ लिखी हैं। कुल मिलाकर, नर्मदा ने भौतिक रूप से नगरों को बसाया, अर्थव्यवस्था को संवारा और अध्यात्मिक रूप से जनमानस को जोड़ा है। भारतीय समाज और संस्कृति की नींव में नर्मदा की अविरल धारा का अमूल्य योगदान रहा है।
ऐतिहासिक महापुरुषों का जुड़ाव

नर्मदा नदी अनेक संतों, साधकों और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की तपस्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य (8वीं सदी) ने अपनी ज्ञान की खोज में बाल्यकाल में नर्मदा पर कदम रखा। केरल से हज़ारों किलोमीटर पदयात्रा कर वे ओंकारेश्वर पहुंचे, जहाँ नर्मदा तट पर स्थित एक गुफा में उन्हें गुरु गोविंद भगवत्पाद मिले। ओंकारेश्वर में गुरुदेव के सान्निध्य में रहकर शंकराचार्य ने चार वर्षों तक अद्वैत वेदांत की शिक्षा ग्रहण की तथा नर्मदाष्टकं जैसी स्तुतियों की रचना की। एक प्रचलित कथा है कि गुरु की परीक्षा लेने हेतु स्वयं नर्मदा ने भीषण बाढ़ का रूप लिया, तब शंकराचार्य ने अपने कमंडलु में उस बाढ़ के जल को धारण कर नदी को शांत किया था – इस चमत्कार से प्रभावित होकर गुरु ने उन्हें ज्ञानदान दिया। आज भी ओंकारेश्वर में वह गुफा (गुरु-शिष्य गुफा) दर्शनीय है, जहाँ शंकराचार्य ने तपस्या की थी। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊँची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित की है, जो इस ऐतिहासिक मिलन की स्मृति दिलाती है।
भक्तिकाल के महान संत कबीर का भी नर्मदा से विशेष नाता रहा है। कबीरदास (15वीं सदी) ने जीवन भर सत्यमार्ग का प्रसार किया और देशभर में यात्राएँ कीं। गुजरात में भरूच के निकट नर्मदा नदी के बीच स्थित कबीरवड द्वीप पर कबीर ने तपस्या की थी। वहाँ एक वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न कबीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसी लोकमान्यता है। आज उस द्वीप पर फैला विशाल बरगद का पेड़ कबीर की स्मृति से जुड़ा हुआ है – कहते हैं कि वह पेड़ कबीर द्वारा लगाए गए दातून की डाल से ही पनपा था। कबीरवड तीर्थ पर कबीरपंथियों द्वारा वार्षिक उत्सव आयोजित होता है और एक मंदिर भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानकदेव ने भी नर्मदा तट की यात्रा की थी। गुरु नानक के चरण जबलपुर के ग्वारीघाट पर पड़े, जहाँ आज गुरुद्वारा ग्वारीघाट उनकी याद में स्थित है। गुरु नानक ने नर्मदा के सौंदर्य और निर्मलता का बखान अपने शब्दों में किया है। कई अन्य संत-महात्माओं ने भी नर्मदा की महिमा गायी है – दयानंद सरस्वती ने नर्मदा पर विविध तीर्थों का भ्रमण किया था, स्वामी विवेकानंद ने अपनी भारत यात्रा के दौरान अमरकंटक और ओंकारेश्वर में ध्यान किया था, और संत तुकाराम वnamdev जैसे मराठी संतों ने भी नर्मदा तट पर भजन-कीर्तन किए थे।
नर्मदा तट प्राचीन ऋषि-मुनियों की तपोभूमि तो थी ही, मध्यकालीन संतों और तपस्वियों ने भी यहां आश्रय लिया। भगवान परशुराम से जुड़ी कथाएँ महिष्मती (महेश्वर) क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ उन्होंने सहस्रार्जुन का वध किया था – आज महेश्वर का सहस्रधारा स्थल उसी कथा का द्योतक है। कपिल मुनि ने अमरकंटक में नर्मदा तट पर ही तप कर कपिलधारा की स्थापना की। मार्कंडेय ऋषि ने भी नर्मदा तट पर यज्ञ किया था – गुजरात में अंकलेश्वर के पास उनके नाम पर मार्कंडेय आश्रम है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान नर्मदा के जंगलों (मैकल पर्वत श्रेणी) में शरण ली थी, ऐसी कथाएँ स्कंदपुराण में मिलती हैं। आधुनिक काल में निरंतर कई संत नर्मदा परिक्रमा करते रहे हैं, जिनमें करपात्री महाराज, सोमवारी बाबा, प्रमथनंद जी जैसे तपस्वी प्रसिद्ध हैं। संत रामदास, गोंविदसिंह आदि ने भी नर्मदा की पैदल यात्रा का वृत्तांत लिखा है।
समग्रतः, नर्मदा नदी ज्ञान, भक्ति और तप की धारा को अपने साथ बहाती आई है। आदि शंकराचार्य जैसे दार्शनिक से लेकर कबीर जैसे संत तक – सभी ने इससे प्रेरणा पाई। आज भी नर्मदा किनारे साधु-संतों के आश्रम देखे जा सकते हैं और परिक्रमा मार्ग पर सैकड़ों तपस्वी मिलते हैं। नर्मदा की गोद में अध्यात्म की जो धारा प्रवाहित हुई, उसने भारतीय संस्कृति के महान पुरुषों को गढ़ने में अहम भूमिका निभाई है। नर्मदा सचमुच “श्रद्धा और सभ्यता की नदी” है – जिसके तट पर इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म सभी एक साथ प्रवाहमान हैं।
लेखक – देवऋषि, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक शोधकर्ता